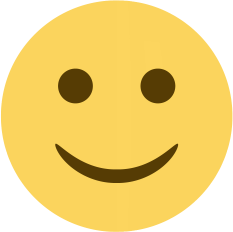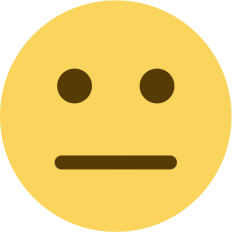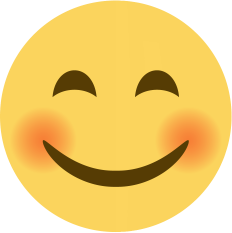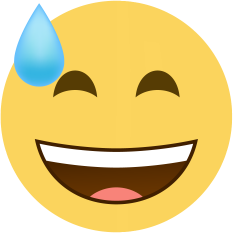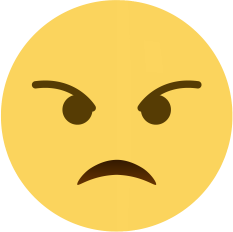रुक नहीं रहे बाल विवाह : एक वैश्विक सामाजिक सरोकार

डॉ. आर. एच. लता
बाल विवाह, यानी वयस्कता प्राप्त करने से पूर्व बच्चों का विवाह, आज भी विश्वभर में एक गम्भीर सामाजिक समस्या के रूप में विद्यमान है। यह प्रथा न केवल बच्चों के अधिकारों का हनन करती है, बल्कि उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह में भी बाधा उत्पन्न करती है। 21वीं सदी में जब मानवाधिकार, लैंगिक समानता और बच्चों के भविष्य को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, तब भी बाल विवाह जैसी परंपराएँ कई देशों में आज भी जीवित हैं।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के अनुसार, आज भी विश्व में हर पाँच में से एक लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है। विशेषकर दक्षिण एशिया, उप-सहारा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में बाल विवाह की घटनाएँ अत्यधिक हैं। भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में विश्व के बाल विवाह मामलों का लगभग आधा हिस्सा पाया जाता है। वहीं, नाइजर, चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य जैसे अफ्रीकी देशों में यह दर 70 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है। लैटिन अमेरिकी देशों में भी गरीबी और सामाजिक असमानता के कारण बाल विवाह का चलन बना हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि यह समस्या किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक चुनौती है।
बाल विवाह के पीछे कई गहरे कारण हैं। निर्धनता और आर्थिक असुरक्षा के कारण अनेक परिवार लड़कियों का शीघ्र विवाह कर देने को विवश हो जाते हैं। समाज में लड़कियों को अब भी अनेक स्थानों पर पुरुषों की तुलना में कमतर माना जाता है, जिससे वे अपने भविष्य के निर्णय लेने से वंचित रह जाती हैं। युद्ध, आपदाएँ और विस्थापन जैसी परिस्थितियाँ भी कई बार बाल विवाह को बढ़ावा देती हैं, जब माता-पिता असुरक्षा की भावना से बेटी की जल्दी शादी करना उचित समझते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक क्षेत्रों में सामाजिक परंपराओं और धार्मिक विश्वासों के चलते भी यह प्रथा आज तक बनी हुई है। इस कुप्रथा के दुष्परिणाम अत्यंत गंभीर हैं। किशोर अवस्था में विवाह और गर्भधारण से मातृत्व सम्बन्धी जटिलताएँ बढ़ जाती हैं और माँ व शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर संकट उत्पन्न होता है। विवाह के बाद लड़कियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, जिससे उनका आत्मनिर्भर बन पाना कठिन हो जाता है। घरेलू हिंसा, शोषण और मानसिक उत्पीड़न की शिकार भी अनेक बाल वधुएँ होती हैं। जब एक पीढ़ी शिक्षा और अवसरों से वंचित रह जाती है, तो गरीबी और पिछड़ेपन का दुष्चक्र अगली पीढ़ी तक चला जाता है। हालाँकि इस दिशा में वैश्विक स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपने सतत विकास लक्ष्यों में 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। यूनिसेफ और यूएनएफपीए जैसे संगठनों द्वारा कई देशों में कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। 'गर्ल्स नॉट ब्राइड्स' जैसे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बाल विवाह के विरुद्ध जन-जागरूकता और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही, अनेक देशों ने विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करते हुए कड़े कानून भी बनाए हैं।
सामाजिक सोच और व्यवहार में बदलाव आवश्यक :
भारत ने भी इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। शिक्षा, सरकारी योजनाओं और सामाजिक अभियान जैसे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के माध्यम से बाल विवाह की दर में कमी आई है। फिर भी, भारत अब भी उन देशों में शामिल है जहाँ बाल वधुओं की संख्या सर्वाधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि सामाजिक सोच और व्यवहार में बदलाव भी उतना ही आवश्यक है।
आज बाल विवाह केवल कानूनी अपराध नहीं, बल्कि यह एक गम्भीर सामाजिक सरोकार है जो मानवाधिकार, लैंगिक न्याय और समान अवसरों से जुड़ा हुआ है। इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक है कि बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए, निर्धन परिवारों को आर्थिक सहयोग मिले और सामाजिक स्तर पर बाल विवाह के विरुद्ध चेतना जगाई जाए। जब तक हम समाज के हर वर्ग को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक यह कुप्रथा जड़ से समाप्त नहीं हो सकेगी।
अंततः, यदि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जो समानता, स्वतंत्रता और मानव गरिमा के मूल्यों पर आधारित हो, तो बाल विवाह जैसी प्रथाओं को जड़ से समाप्त करना होगा। यह केवल सरकारों या संस्थाओं का ही नहीं, हम सबका साझा दायित्व है।
(लेखिका पूर्व सदस्य, मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग हैं)
 प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस
प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस